
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस (निम्हंस) ने 2016 में देश के 12 राज्यों में एक सर्वेक्षण करवाया था. इसके बाद कई चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं.
आंकड़ों के मुताबिक आबादी का 2.7 फ़ीसदी हिस्सा डिप्रेशन जैसे कॉमन मेंटल डिस्ऑर्डर से ग्रसित है.
जबकि 5.2 प्रतिशत आबादी कभी न कभी इस तरह की समस्या से ग्रसित हुई है.
इसी सर्वेक्षण से एक अंदाजा ये भी निकाला गया कि भारत के 15 करोड़ लोगों को किसी न किसी मानसिक समस्या की वजह से तत्काल डॉक्टरी मदद की ज़रूरत है.
साइंस मेडिकल जर्नल लैनसेट की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 ज़रूरतमंद लोगों में से सिर्फ़ एक व्यक्ति को डॉक्टरी मदद मिलती है.

ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में मानसिक समस्या से ग्रसित लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. और आने वाले दस सालों में दुनिया भर के मानसिक समस्याओं से ग्रसित लोगों की एक तिहाई संख्या भारतीयों की हो सकती है.
जानकार ये आशंका जताते हैं कि भारत में बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं. शहर फैल रहे हैं, आधुनिक सुविधाएं बढ़ रही हैं. बड़ी संख्या में लोगों का गांवों से पलायन हो रहा है. इन सब का असर लोगों के मन मस्तिष्क पर भी पड़ सकता है. लिहाज़ा डिप्रेशन जैसी समस्या के बढ़ने की आशंका है.
दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ़ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज़ (इब्हास) के निदेशक डॉक्टर निमीश देसाई का कहना है, “भारत में परिवारों का टूटना, स्वायत्ता पर ज़ोर और टेक्नॉलॉजी जैसे मुद्दे लोगों को डिप्रेशन की ओर धकेल रहे हैं क्योंकि समाज पाश्चात्यकरण की ओर टॉप फाइव गियर में बढ़ रहा है, ये बीसवीं सदी का पोस्ट वर्ल्ड वार का सोशल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का मॉडल है. यहां सवाल ये उठता है कि क्या गुड डेवलपमेंट ज़रूरी है या गुड मेंटल हेल्थ ज़रूरी है?”
डॉक्टर निमीश हालांकि इसे लेकर आश्वस्त भी हैं कि लोगों में अब मेंटल हेल्थ की अहमियत की समझ पैदा होने लगी है लेकिन वे यह भी मानते हैं कि समाज का एक तबका इस पर खुल कर बातें करना पसंद नहीं करता और इसे एक टैबू के तौर पर लेता है.
2015 में हिंदी फ़िल्मों की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने एक न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में बताया था कि वे डिप्रेशन की शिकार हुई थीं. उन्हें अभिनय के लिए काफी प्रशंसा मिल रही थी, अवार्ड्स मिल रहे थे लेकिन एक सुबह उन्हें लगा कि उनका जीवन दिशाहीन है, वे लो फील करती थीं और बात-बात पर रो पड़ती थीं.
क्या होता है कॉमन मेंटल डिस्ऑर्डर?
दिल्ली स्थित सेंट स्टीफ़न अस्पताल में मनोचिकित्सक डॉक्टर रूपाली शिवलकर का कहना है कि कॉमन मेंटल डिसऑर्डर या सीएमडी से 30-40 फ़ीसदी लोग प्रभावित हैं और लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि वो एक बीमारी हैं.
सीएमडी के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं. जैसे, किसी भी काम में मन न लगना, शरीर में कोई बीमारी न होने के बावजूद थकान महसूस करना, नींद आते रहना, बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सा या रोने का मन करना आदि.
वहीं, बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव, स्कूल जाने के लिए मना करना, गुस्सैल हो जाना, आलसी हो जाना या बहुत एक्टिव हो जाना.
अगर ये लक्षण लगातार दो हफ़्ते तक रहते हैं तो ये सीएमडी की ओर इशारा करते हैं.
डॉक्टर रुपाली शिवलकर बताती हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की हॉर्मोनल दिक्कत, हाइपरथॉइरॉडिज़्म, डायबीटिज़ या क्रोनिक यानि लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित होता है तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रुरत पड़ती है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन या डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया भर में 10 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं और बच्चा पैदा करने के बाद 13 प्रतिशत महिलाएं डिप्रेशन से गुजरी हैं.
वहीं, विकासशील देशों में आंकडा ऊपर हैं जिसमें 15.6 गर्भवती और 19.8 प्रतिशत डिलीवरी के बाद डिप्रेशन से गुजर चुकी है. बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं.
भारत में 0.3 से लेकर 1.2 फीसदी बच्चे डिप्रेशन में घिर रहे हैं और अगर इन्हें समय रहते नहीं डॉक्टरी मदद नहीं मिली तो सेहत और मानसिक स्वास्थ्य संबधी जटिलताए बढ़ सकती हैं.

बढ़ रही है मानसिक रोगियों की संख्या?
दिल्ली स्थित भारतीय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में मनोचिकित्सा विभाग में डॉक्टर नंद कुमार का कहना है कि 10 साल पहले मनोचिकित्सक ओपीडी में 100 मरीज आते थे लेकिन अब रोज़ 300-400 लोग आते है.
वहीं इब्हास के अध्यक्ष का कहना था कि आज से 10-15 साल पहले जहां 100-150 लोग आते थे वहीं अब 1200-1300 लोग रोज़ आते हैं
बच्चों की मानसिक सेहत
इनमें ज़्यादातर लोग सीएमडी का ही शिकार होते हैं. इनमें बच्चे और युवा उदासी, आत्मविश्वास में कमी, गुस्सा, चिड़चिड़पन जैसी समस्याओं के साथ आते हैं वहीं महिलाएं थकान, घबराहट अकेलापन की समस्याएं लेकर आती हैं.
डॉक्टरों का कहना है कि सोशल मीडिया भी किशोरों या युवाओं को डिप्रेशन की ओर ले जाने का कारण बनता है.
डॉक्टर नंद किशोर का कहना है, सोशल मीडिया पर आपके पोस्ट या फ़ोटो को लाइक या डिस्लाइक किया जा रहा है या कोई एक्सप्रेशन न आना आपको रिजेक्ट या डिजेक्ट होने का एहसास दिलाता है जिससे एक तरह से भावनात्मक बोझ बढ़ जाता है.
इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रुपाली शिवलकर कहती हैं कि आजकल बच्चों पर कई तरह के परफॉर्मेंस का दबाव हैं जहां माता-पिता बच्चों से पढ़ाई लिखाई के अलावा अन्य गतिविधियों संगीत, डांस, खेल, एक्टिंग आदि में बेहतरीन होने की उम्मीद करते हैं.
दूसरी तरफ बच्चों में पीयर प्रेशर, सोशल साइट्स पर नए नए स्टेटस अपडेट करने का दबाव उनके सामने अस्तित्व का सवाल पैदा कर देता है.
वहीं, आज के ज़माने में उनके सामने विकल्प ज्यादा होना या एक्सपोजर ज़्यादा है जो उन्हें और स्ट्रेसफुल बना देता है.
यह दवाब सिर्फ़ बच्चों और किशोरों तक सीमित नहीं है. इसके दुष्प्रभाव गंभीर हो सकते हैं. डॉक्टरों का कहना है कि कई बार लोगों के जीवन में डिप्रेशन या तनाव इतना बढ़ जाता है कि लोग आत्महत्या का कदम भी उठा लेते हैं.
विश्व स्वास्थ्य संगठन या डब्लूएचओ ने इस साल 2019 के लिए ‘आत्महत्या की रोकथाम’ को थीम रखा है.
डब्लूएचओ के मुताबिक हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में 800,000 लोग आत्महत्या करते हैं.
संस्था के मुताबिक 15 -29 उम्र वर्ग के युवाओं में आत्महत्या मौत का दूसरा बड़ा कारण है.
गौर करने वाली बात ये है कि यह विकसित देशों की समस्या नहीं है बल्कि करीब 80 फ़ीसदी आत्महत्याएं निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती है.
डॉक्टरों का कहना है कि आत्महत्या को रोका जा सकता है और एक बार आत्महत्या करने वाला व्यक्ति दोबारा भी कोशिश करता है. इसके शुरुआती लक्षण होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है.
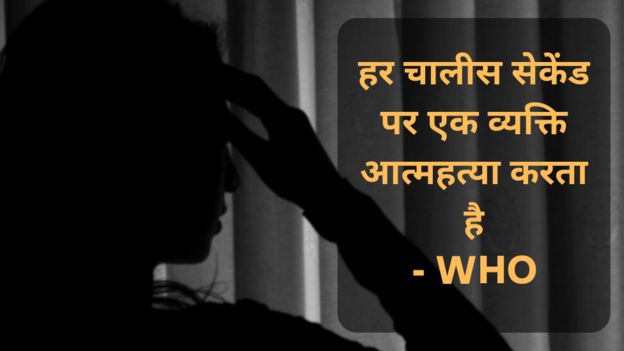
एक आत्महत्या से कितने प्रभावित?
डॉक्टर नंद कुमार का कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति आत्महत्या करता है उसके साथ साथ 135 लोग प्रभावित होते हैं. इनमें आत्महत्या करने वाला परिवार, निकट परिजन, रिश्तेदार, दोस्त और ऑफ़िस में काम करने वाले शामिल हैं. इसलिए किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने से पहले इन लोगों के बारे में सोचना ज़रूरी है.
उनके अनुसार, आत्महत्या आवेग में लिया गया कदम है. अगर आप उन चंद सेकेंड्स में आत्महत्या करने वाले को डाइवर्ट कर सकते हैं तो आप उसकी जान बचा सकते हैं.
डब्ल्यूएचओ आत्महत्या को रोकने के लिए कई सुझाव देता है. इनमें पहले पहल आत्महत्या को एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या मान कर जागरूकता लाना शामिल है. जो इस समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें इस बात का एहसास दिलाना भी ज़रूरी है कि वो खुद को अकेला न समझें.
समस्या गंभीर हैं लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि लोगों में अब मानसिक सेहत को लेकर जागरूगता आई है. लेकिन ये जागरूकता फिलहाल शहरों तक सीमित है.
डॉ रूपाली बताती है कि गांवों में कॉमन मेंटल डिस्ऑर्डर के बारे में लोग ध्यान भी नहीं देते और इसे बीमारी भी नहीं समझते लेकिन अगर कोई व्यक्ति सीवियर मेंटल डिस्ऑर्डर यानी स्किजोफ़्रीनिया, अल्ज़ाइमर और डिमेंशिया से पीड़ित होता है तो वे उसकी डॉक्टरी इलाज करवाते हैं क्योंकि उसके लक्षण साफ़ दिखाई देते हैं.
ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता
डॉक्टर मानते हैं कि भारत जैसे देश में निम्न आय वर्ग या ग्रामीण इलाकों में लोग एनिमिया, कुपोषण या डायरिया जैसी बीमारी से जूझ रहे हो वहां उनका ध्यान मेंटल हेल्थ पर कैसे जा पाएगा.
इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार की तरफ से मेंटल हेल्थकेयर एक्ट 2017 लाया गया. इससे पहले साल 1987 में क़ानून लाया गया था. नए क़ानून के तहत केंद्र सरकार ने दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति को अधिकार देने की बात की है.
आत्महत्या को पहले एक जुर्म माना जाता था लेकिन नए क़ानून ने इसे जुर्म के दायरे से बाहर निकाल दिया गया है और सभी पीड़ितों को इलाज का अधिकार दिया गया है. राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के गठन का भी प्रावधान है.

डॉक्टर नीमिश देसाई का कहना है कि क़ानूनी बदलाव स्वागत योग्य है लेकिन वो और प्रभावी हो सकते थे. इनमें पश्चिमी देशों की नकल ज़्यादा है जबकि भारत में मेंटल हेल्थ की समस्या वैसी नहीं है जैसे पश्चिमी देशों में है. भारत की सामाजिक और पारिवारिक बनावट इस समस्या से निपटने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं.
लेकिन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल यानी मनौवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक की ज़रूरत पर कोई शक नहीं है.
अमरीका में जहां 60-70 हज़ार मनोचिकित्सक हैं वहीं भारत में ये संख्या 4 हज़ार से भी कम है. जबकि यहां इस वक्त 15 से 20 हज़ार मनोचिकित्सकों की ज़रूरत है.
देश में फिलहाल 43 मेंटल अस्पताल हैं जिनमें से दो या तीन सुविधाओं के स्तर पर बेहतर माने जाते हैं, 10-12 में सुधार हो रहा है जबकि 10-15 अभी भी कस्टोडियल मेंटल हॉस्पिटल बने हुए हैं.
डॉक्टरों का ये भी मानना है कि एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान ही मनोचिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए.
वहीं, दूसरी तरफ मानसिक समस्या से पीड़ितों की पहचान के लिए व्यापक स्क्रीनिंग शुरू की जानी चाहिए क्योंकि अगर इस पर जल्द क़ाबू न पाया गया तो एक दशक में यह एक महामारी का रूप ले सकती है.——-बीबीसी हिन्दी
